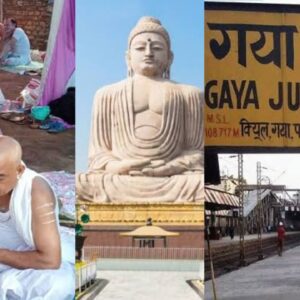सीपीआई(एम) के आगामी 24वें कांग्रेस से पहले पार्टी की पोलित ब्यूरो द्वारा जारी एक आंतरिक नोट, जिसे मीडिया में प्रमुखता से रिपोर्ट किया गया है, पर पहले जारी हुए मसौदा प्रस्ताव से कहीं ज्यादा चर्चा हो रही है. इस मसौदे में दो जगहों पर मौजूदा राजनीतिक हालात और मोदी सरकार को “नव-फ़ासीवादी लक्षणों” वाला बताया गया है. इस आंतरिक नोट में स्पष्ट किया है कि “नव-फ़ासीवादी लक्षणों” का अर्थ केवल कुछ ख़ास विशेषताएँ या रुझान हैं, और मोदी सरकार किसी भी तरह से फ़ासीवादी या नव-फ़ासीवादी नहीं है. नोट यह भी स्पष्ट करता है कि देश के मौजूदा हालात के विश्लेषण में सीपीआई(एम) की स्थिति सीपीआई और सीपीआई(एमएल) से भिन्न है.
शायद ‘नव-फ़ासीवाद’ शब्द के प्रयोग ने सीपीआई(एम) के कार्यकर्ताओं में यह भ्रम पैदा कर दिया कि सीपीआई(एम) और सीपीआई(एमएल) के बीच मुख्य मतभेद सिर्फ़ ‘नव’ शब्द के इस्तेमाल तक सीमित है. इसी कारण नोट में यह स्पष्ट करने की ज़हमत उठानी पड़ी कि फिलहाल भारत में फ़ासीवाद केवल एक प्रवृत्ति के रूप में मौजूद है. इसके लक्षण अभी विकासमान हैं, लेकिन ये इतने मजबूत या निर्णायक नहीं हैं कि सत्ता को पूरी तरह फ़ासीवादी कहा जा सके. इस नोट का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पार्टी ‘नव-फ़ासीवादी’ शब्द को अधिक महत्व न दे, जो पहली बार सीपीआई(एम) के किसी दस्तावेज़ में इस्तेमाल किया गया है. दूसरे शब्दों में, हालात ऐसे हैं कि अब ‘फ़ासीवाद’ शब्द को नज़रअंदाज़ करना संभव नहीं है, इसलिए यह नोट पार्टी को चेतावनी दे रहा है कि इस खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर आँकने की गलती से बचना चाहिए.
नोट में इटली और जर्मनी में उभरे फ़ासीवाद को ‘शास्त्रीय फ़ासीवाद’ कहा गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि उभरता हुआ ‘नव-फ़ासीवाद’ इससे किस तरह अलग है. इन अंतरों का एक हिस्सा परिस्थितियों से जुड़ा है—इटली और जर्मनी में फ़ासीवाद पहले विश्व युद्ध के बाद उस समय उभरा जब साम्राज्यवादी ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा और चरम टकराव के कारण विश्व युद्ध हुए और पूंजीवाद गहरे संकट में चला गया, जिसे आज हम महामंदी के नाम से जानते हैं. लेकिन नोट यहीं नहीं रुकता, बल्कि एक और फ़र्क की ओर इशारा करता है, जो ज़्यादा बुनियादी है — कि पुराने फ़ासीवाद ने पूंजीवादी लोकतंत्र का पूरी तरह निषेध कर दिया था, वहीं ‘नव-फ़ासीवाद’ पूंजीवादी लोकतंत्र, ख़ासकर चुनावी प्रणाली, के साथ सहज और सुसंगत है. दूसरे शब्दों में, पुराने फ़ासीवाद में कोई आंतरिक नियंत्रण नहीं था और इसने लोकतंत्र के हर हिस्से को तहस-नहस करने वाला विनाशकारी तूफ़ान खड़ा कर दिया था, लेकिन नव-फ़ासीवाद में कहीं न कहीं एक आत्म-संयम या आत्म-नियंत्रण की प्रवृत्ति दिखती है.
पुराने फ़ासीवाद और उसके ‘नव’ रूप के बीच किए जा रहे इस फर्क पर गहराई से गौर करने की ज़रूरत है, सीपीआई(एम) के इस दावे पर भी कि भारत में अभी जो कुछ देखा और अनुभव किया जा रहा है वह सिर्फ़ कुछ ‘नव-फ़ासीवादी प्रवृत्तियाँ’ हैं जो यदि अनियंत्रित रहीं तो भविष्य में नव-फ़ासीवाद का रूप ले सकती हैं. यदि हम 1920 के दशक में फ़ासीवाद के उदय के ऐतिहासिक संदर्भ पर गौर करें तो इसमें साम्राज्यवादी ताकतों के बीच तीखे टकराव और आर्थिक संकट से भी बड़ा एक और कारण था — क्रांति का डर. काफी पहले 1848 में प्रकाशित ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ की शुरुआत जिन ऐतिहासिक शब्दों से हुई थी — ‘यूरोप में एक भूत मंडरा रहा है— कम्युनिज़्म का भूत’, नवंबर 1917 में रूसी क्रांति की जीत के बाद इस भूत के हक़ीक़त बन जाने का ख़तरा और भी बढ़ गया था. हालाँकि, यूरोप के देशों में क्रांतिकारी संभावनाएँ साकार नहीं हो सकीं, रूसी क्रांति की पाँचवीं वर्षगांठ आते—आते फ़ासीवाद इटली में सत्ता हासिल कर चुका था.
यूरोप में फ़ासीवाद के शुरुआती दौर में ही यह साफ़ हो गया था कि यह भले ही एक अंतरराष्ट्रीय परिघटना हो, लेकिन हर देश की ऐतिहासिक परिस्थितियों और सामाजिक हालात के अनुसार इसका राष्ट्रीय स्वरूप अलग-अलग होगा. जर्मनी में जब फ़ासीवाद उभार हुआ, उससे पहले ही उसे वहां एक नया नाम मिला चुका था— नाज़ीवाद या राष्ट्रीय समाजवाद. आज भारत में कोई भी बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में यूरोप में देखे गए फ़ासीवादी मॉडल की हूबहू नकल की बात नहीं कर रहा है. आज के भारत के माक्र्सवादी विश्लेषण के लिए यहाँ की मूलभूत विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए इतिहास में फ़ासीवाद की सभी परिघटनाओं के बीच की बुनियादी समानताओं को लेकर आगे बढ़ना होगा. इसी संदर्भ में सीपीआई(एम) के स्पष्टीकरण नोट पर विचार करना चाहिए.
सीपीआई(एम) भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस व्यापक प्रगतिशील राय से सहमत है जो आरएसएस को फ़ासीवादी मानती है. यह महत्वपूर्ण है कि अपनी स्थापना के समय से ही आरएसएस ने इटली और जर्मनी के “क्लासिकल मॉडल” से काफ़ी कुछ ग्रहण किया — विचारधारात्मक आधार, संगठनात्मक ढाँचा और काम करने का तरीका. जिस तरह जर्मनी में यहूदियों को आंतरिक दुश्मन के रूप में चिन्हित किया गया था, उसी तरह भारत में आरएसएस ने मुसलमानों को ‘असली आंतरिक दुश्मन’ के रूप में चिन्हित किया. यह अलग बात है कि औपनिवेशिक भारत न तो युद्धोत्तर इटली जैसा था और न ही जर्मनी जैसा. इटली और जर्मनी में फ़ासीवादी अपने उदय के कुछ ही वर्षों में सत्ता में आ गए थे, लेकिन भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और फिर संवैधानिक गणतंत्र बनने के शुरुआती दशकों में आरएसएस हाशिए की ताक़त बना रहा.
शायद दुनिया में फ़ासीवादी प्रवृत्ति का ऐसा कोई और उदाहरण नहीं है, जो इतने लंबे समय तक खुद को टिकाए रख सका हो, बदलती सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालते हुए ताकत जमा करता रहा हो और गणतंत्र के संस्थागत ढाँचे में चुपके से घुसपैठ करके आज वह आरएसएस जैसी पकड़ और वर्चस्व हासिल कर सका हो. सवाल यह है कि कोई फ़ासीवादी ताक़त, जब उसे राजनीतिक सत्ता पर इतनी मज़बूत पकड़ मिल जाए, तो वह अपने पूरे फ़ासीवादी एजेंडे को खुलकर लागू करने की ओर बढ़ेगी या फिर पूंजीवादी लोकतंत्र के दायरे में बनी रहेगी और उसके तथाकथित नियमों के अनुसार चलेगी? आरएसएस का पिछले सौ सालों का इतिहास — इसके उतार-चढ़ाव, रणनीतिक तौर पर पीछे हटने और आगे बढ़ने — खासतौर पर पिछले चार दशकों में इसे तेज़ी से मिला उभार और मज़बूती, इस बात पर किसी के मन में ज़रा भी संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ता.
आडवाणी की रथयात्रा और बाबरी मस्जिद विध्वंस
आडवाणी की रथयात्रा के ज़रिए राम जन्मभूमि अभियान को मिली तीव्रता और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने की घटना ने पहली बार हमें संघ ब्रिगेड के खुलेआम फ़ासीवादी इरादों की साफ़ झलक दिखा दी थी. यह सिर्फ़ उग्र सांप्रदायिकता या कट्टरपंथी उन्माद नहीं था, बल्कि हिंदू वर्चस्व के आधार पर भारत की नयी पहचान गढ़ने और ‘हिंदू राष्ट्र’ की परिकल्पना को साकार करने की सोची-समझी कोशिश थी. भाकपा(माले) ने इसे भारत की समावेशी संस्कृति और संवैधानिक जनतंत्र के लिए सांप्रदायिक फ़ासीवादी खतरे के रूप में पहचाना. कॉमरेड विनोद मिश्रा और सीताराम येचुरी ने आरएसएस की आरएसएस की इस रणनीति पर विस्तार से लिखा और वामपंथी व प्रगतिशील ताक़तों को इस निर्णायक मोड़ के वैचारिक और राजनीतिक प्रभावों को लेकर सचेत भी किया. प्रगतिशील अकादमिकों तपन बसु, सुमित सरकार, प्रदीप दत्ता, तनिका सरकार और सम्बुद्ध सेन ने आरएसएस के फासीवादी चेहरे को बेनकाब करते हुए ‘खाकी शार्ट्स एण्ड सैफ्रन फ्लैग्स’ नाम की एक शानदान पुस्तिका प्रकाशित की.
बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बना भाजपा का अलगाव ज़्यादा समय तक नहीं रहा. महज़ पाँच साल के भीतर ही पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बना लिया. सदी के अंत तक भारत एनडीए के शासन के अधीन आ चुका था, जो अपना कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर-कांग्रेस सरकार थी. जनवरी 1999 में बजरंग दल के नेता दारा सिंह और उसके गुर्गों द्वारा ग्रैहम स्टुआर्ट स्टेन्स और उनके दो बेटों — फिलिप और टिमोथी — की हत्या और तीन साल बाद गुजरात में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए जनसंहार ने संघ परिवार के उजागर होते एजेंडे की ओर साफ इशारा कर दिया था. गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में हुए इस जनसंहार की कड़ी निंदा भारत और विदेशों में हुई, और इसका असर 2004 में एनडीए की हार में साफ़ दिखा. लेकिन संघ-भाजपा नेतृत्व द्वारा नरेंद्र मोदी पर कोई कार्रवाई न करने के फ़ैसले से यह साफ़ हो गया कि संघ परिवार ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य की ओर अगला क़दम बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार था.
यूपीए सरकार ने भले ही दो पूरे कार्यकाल तक शासन किया, लेकिन भाजपा ने गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और कॉरपोरेट जगत भी ‘वाइब्रेंट गुजरात’ नाम के दो साल में एक बार होने वाले निवेश सम्मेलनों के ज़रिए जरिए मोदी ब्रांड के इर्द-गिर्द जमकर जुटने लगा. कॉर्पोरेट भारत के निर्णायक समर्थन से मोदी को दिल्ली लाने की मांग और ज़ोर पकड़ने लगी. अडानी-अंबानी के साथ टाटा समूह भी इस मुहिम में शामिल हो गया, और 2014 में हमने मोदी युग का आगमन देख लिया. यह नहीं भूलना होगा कि कॉरपोरेट और सांप्रदायिक राजनीति के सम्मिलन ने इस रास्ते को बनाया था. धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत को हिंदू वर्चस्ववादी फ़ासीवादी व्यवस्था के अधीन करने के संघी एजेंडे को योजनाबद्ध तरीके से और तेज़ी से लागू किया गया. अगर इसे सिर्फ़ नवउदारवाद के संकट के रूप में देखा जाएगा तो यह पूरी तस्वीर को नहीं देख पायेंगे, क्योंकि फासीवादी तबाही का यह ब्लूप्रिन्ट कहीं ज़्यादा गहरा और व्यापक है.
करीब अस्सी साल पहले, आंबेडकर ने हमें चेतावनी दी थी कि “अगर हिंदू राज हकीकत बन गया, तो यह निस्संदेह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी,” और उनकी यह चेतावनी पूरी तरह सही साबित हो रही है. यह सरकार लोकतंत्र को नष्ट करने और नागरिकों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं को खत्म करने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है — कानूनों में संशोधन करने और कानून व न्याय के ढाँचे को बदलने से लेकर, संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ नए कानून बनाने और जनतंत्र की पूरी संस्थागत व्यवस्था व माहौल को कमजोर करने तक. इसके साथ ही, मुसलमानों, समाज के कमजोर तबकों और असहमति की आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ राज्य-प्रायोजित नफरत और हिंसा को खुली छूट दी जा रही है. यह हमारे लोकतांत्रिक जनतंत्र की संवैधानिक बुनियाद पर अभूतपूर्व हमले की भयावह तस्वीर पेश करता है. अब तो नए संविधान की मांग भी अलग-अलग मंचों से उठने लगी है. खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं सालगिरह पर हुई चर्चा के दौरान बाबासाहेब आंबेडकर के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की.
भारत में चुनाव अभी भी हो रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में हो और मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतगणना तक चुनावी प्रक्रिया लगातार अपारदर्शी और मनमानी होती जा रही हो, तो क्या चुनाव सच में भारत के संकटग्रस्त लोकतंत्र के लिए कोई ठोस सुरक्षा कवच साबित हो सकते हैं? हमें याद रखना चाहिए कि हिटलर भी चुनावी रास्ते से सत्ता में आया था फिर उसने धीरे-धीरे पूरे विपक्ष को अवैधानिक बना 99% वोट हासिल कर स्थायी तानाशाही थोप दी. भारत में, अमित शाह लगातार पचास साल तक शासन करने की बात करते रहते हैं. भाजपा की हरेक चुनाव को जीतने और सत्ता से चिपके रहने की खतरनाक और कुटिल कोशिशों को हम कई बार देख चुके हैं. भारत में चुनाव तेजी से एक तमाशा बनते जा रहे हैं, जो सिर्फ वैश्विक छवि बनाने और देश के भीतर वैधता का दावा करने का एक जरिया भर रह गए हैं.
यह सही है कि भाजपा को अब तक की अपनी राजनीतिक यात्रा में कई सहयोगी और समर्थक मिले हैं. अपने परम्परागत सहयोगियों के समर्थन के अलावा, इसे अक्सर नवउदारवादी एजेंडे और नरम हिंदुत्व की निरंतरता के आधार पर भी व्यापक समर्थन मिलता रहा है. असहमति जताने वालों का उत्पीड़न, इस्लाम को शैतानी रूप में पेश करना, मुसलमानों, अन्य अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े समूहों के खिलाफ नफरत और हिंसा के ज़हरीले अभियान, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन, घटते लोकतांत्रिक दायरे जैसी गंभीर सवालों पर भारत के सार्वजनिक विमर्श में आज भी थोड़ी बहुत संवेदनशीलता और मुखर विरोध दिखता है. कोई आश्चर्य नहीं कि अंबेडकर ने संविधान को अलोकतांत्रिक जमीन पर लोकतंत्र की सतही परत बताया था. इसीलिए कम्युनिस्टों के लिए यह और ज़रूरी हो जाता है कि वे फासीवाद के ख़िलाफ़ प्रतिरोध खड़ा करने में नेतृत्व करें और बढ़ते फासीवादी हमलों के सामने लोकतंत्र के सबसे दृढ़ और प्रतिबद्ध चैंपियन बनकर सामने आएँ.
सीपीआई(एम) के मसौदा प्रस्ताव में कुछ नव-फ़ासीवादी लक्षणों को स्वीकार किया गया है, और नोट में कहा गया है कि अगर इन पर रोक नहीं लगी, तो ये पूर्ण रूप से ‘नव-फ़ासीवाद’ का रूप ले सकते हैं. इस नोट में ‘प्रोटो नव-फ़ासीवाद के अवयवों’ जैसे नये विशेषणों का इस्तेमाल करके और भी स्पष्ट करने की कोशिश की गई है जिसका मतलब शायद यह है कि अभी भी हमारे पास समय है जब तक ये ‘प्रोटो अवयव/तत्व’, जो ‘शास्त्रीय फ़ासीवाद’ से अभी तीन कदम पीछे हैं, 21वीं सदी में फ़ासीवाद के पूर्ण उदाहरण में विकसित हो जाएँ. लेकिन यदि दिशा पहले से तय है और सवाल केवल इस बात का है कि फासीवादी खतरे की तीव्रता कितनी है, तो क्या कम्युनिस्टों के लिए यह संभव है कि वे जो हो चुका है और जो हर दिन हमारे सामने हो रहा है उसे नजरअंदाज कर दें? क्या वे भारत में अभी भी बचे हुए लोकतंत्र से संतोष कर सकते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि यह अब भी मुसोलिनी के इटली या हिटलर के जर्मनी से बेहतर स्थिति में है? अगर भारत में फासीवाद धीरे-धीरे बढ़ा है, तो इसका मुख्य कारण भारत की विशालता और अंर्तनिहित विविधता है, और मोदी शासन इस विविधता को अपने ‘एक राष्ट्र’ के एकरूपता के सिद्धांत से कुचलने में कोई समय नहीं गंवा रही है.]
(लेखक भाकपा माले के महासचिव हैं। )